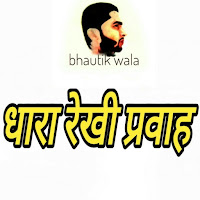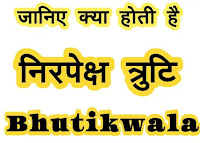प्रश्न - अम्ल क्या हैं ? ये कितने प्रकार के होते हैं ? अम्लों के गुण तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए।
अम्ल की परिभाषा -
 |
अम्लों के प्रकार-
- कार्बनिक या प्रकृति प्रदत्त अम्ल
- अकार्बनिक या खनिज अम्ल
कार्बनिक अम्ल-
- प्याज में एस्कार्बक अम्ल ,
- सेब में मैलेइक अम्ल ,
- दही में लैक्टिक अम्ल ,
- इमली में टार्टरिक अम्ल ,
- सिरके में एसिटिक अम्ल ,
- कोल्ड ड्रिंक में कार्बोनिक अम्ल ,
- संतरे में सिट्रिक अम्ल ,
- टमाटर में ऑकसिलिक अम्ल।
🌑अभिक्रियाऐं🌑
धातुओं के साथ अभिक्रिया -
प्रकृति प्रदत्त अम्ल बहुत ही तनु अम्ल होते हैं इसलिए यह अम्ल बहुत मन्द गति से धातुओं के साथ अभिक्रिया करके विषैले योगिक बनाते हैं। जैसे कि हम नींबू के जूस में एल्यूमिनियम फॉइल का एक छोटासा टुकड़ा डाल देते हैं तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले ऊपर उठते है, यानि कि नींब के जूस ने सिल्फर फॉइल के उस छोटे टुकड़े के साथ अभिक्रिया की।
क्षारकों के साथ आभिक्रिया -
प्रकृति प्रदत्त अम्ल धातुओं की तरह ही क्षारकों से बहुत मन्द गति से अभिक्रिया करते हैं। परन्तु यह इन अम्ल व क्षारकों के अभिक्रियाओं का परिणाम धातुओं वाली अभिक्रिया से भिन्न होता है जिसमें हाइड्रोजन गैसके बुलबुलों की जगह हमें लवण अथवा जल प्राप्त होता है।
खनिज अम्ल (Mineral Acids) -
खनिज अम्ल, खनिजों से तैयार किए जाते हैं। खनिज अम्ल, अधिकांशतः प्रबल अम्ल होते हैं; जैसे-सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और फॉस्फोरिक अम्ल आदि कुछ सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले खनिज अम्ल हैं। खनिज अम्लों का उपयोग उर्वरक, औद्योगिक रसायन, विस्फोटक, रंग तथा रंजक आदि बनाने में किया जाता है। खनिज अम्लों में से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आमाशय में उपस्थित भोजन के पाचन में सहायता करता है।
अधिकांश खनिज अम्ल संक्षारक होते हैं तथा त्वचा पर जलन उत्पन्न करते हैं। अतः इन अम्लों का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। इन अम्लों को छूना या चखना नहीं चाहिए तथा तनु अम्लों का ही प्रयोग करना चाहिए।
अम्लों के गुण
(i) स्वाद - अम्ल तथा उनके विलयन का स्वाद खट्टा होता है।
(ii) संक्षारक प्रकृति - सान्द्र खनिज अम्ल जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल जीव ऊतकों, कपड़ों, कागज तथा धातुओं पर संक्षारित करते हैं। इन पर अम्लों की तीव्र अभिक्रिया होती है।
🌑अभिक्रियाऐं🌑
(i) सूचकों पर अभिक्रिया -
सूचक एक ऐसा पदार्थ है जो अम्लीय तथा क्षारकीय माध्यमों में विभिन्न रंग देता है। लिटमस, मेथिल ऑरेन्ज, फिनॉल्फ्थेलिन आदि कुछ सामान्यतया प्रयोग में आने वाले सूचक हैं। अम्ल तथा उनके विलयन नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल और उनके विलयन पीले मेथिल ऑरेन्ज को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। अम्ल और उनके विलयन का फिनॉल्फ्थेलिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
अतः यदि कोई विलयन नीले लिटमस का रंग लाल में परिवर्तित कर देता है, तब यह अम्ल अथवा उसका विलयन होगा।
(ii) धातुओं के साथ अभिक्रिया-
अम्ल अधिकतर धातुओं के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते है तथा हाईड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्रियाशील घातुओं जैसे मैग्नीशियम तथा जिक के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाते हैं।
नोट - उत्कृष्ट और कम क्रियाशील धातुएँ; जैसे ताँबा, चाँदी तथा सोना अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करते।
(iii) कार्बोनेट तथा हाइड्रोजनकार्बनिट के साथ अभिक्रिया-
अम्ल कार्बनेिट और हाइड्रोजनकार्बोनेट को अपघटित करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं।
उदाहरणार्थ- सोडियम कार्बोनेट तथा कैल्सियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं।
(iv) धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया-
अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल देते हैं। अम्लद्वारा बाख का प्रेक्षित प्रभाव समार ऊर्व क्षारक द्धारा अम्ल का प्रेक्षित प्रपान है अम्ल व क्षारक एक दूसरे के
क्षारक के साथ अभिक्रिया - अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेषित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रेषित प्रभाव समाप्त हो जाता है। यानि कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रति विरोधी होते हैं।अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया करने पर यह एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त देते हैं। अथवा अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणामस्वरुप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। अम्ल एवं क्षारक की इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं।
(v) अम्लों का विलयन रूप -
सभी अम्ल जलीय विलयन में स्वतन्त्र हाइड्रोनियम आयन (H3O+) विमुक्त करते हैं। प्रबल अम्ल विलयन में पूर्णतया विघटित हो जाते हैं।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल व्यावसायिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अम्ल हैं। इन अम्लों के कुछ महत्त्वपूर्ण उपयोगों का उल्लेख निम्नलिखित है-
(i) हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (HCI) के उपयोग-
- क्लोराइड तथा क्लोरीन गैस बनाने में,
- यशदीकरण (कलई) से पहले लोहे की चादरों को साफ करने के लिए,
- वस्त्र-उद्योग में कपड़ा रंगने के लिए।
(ii) नाइट्रिक अम्ल (HNO3) के उपयोग-
- उर्वरक, विस्फोटक, रंग तथा औषधि बनाने के लिए,
- सोने तथा चाँदी के शोधन में।
(iii) सल्फ्यूरिक अम्ल (H₂SO₄) के उपयोग
- उर्वरक, धावन पाउडर, प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे बनाने में,
- पेट्रोलियम उद्योग में, शोधन के लिए,
- लेड बैटरियों में (विद्युत अपघट्य के रूप में)।